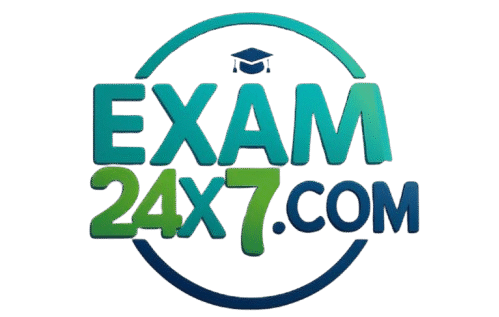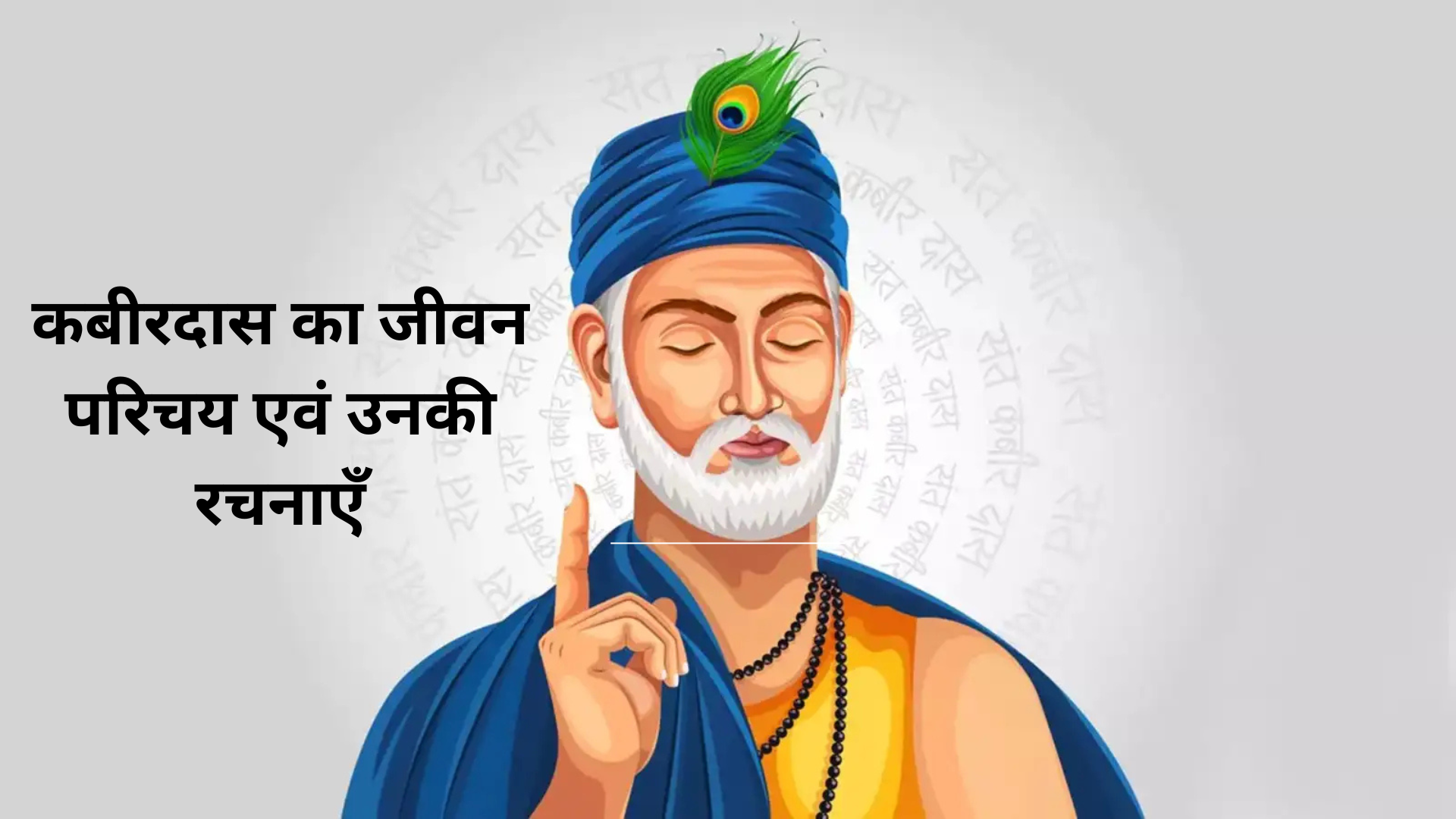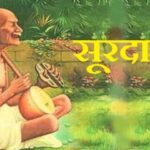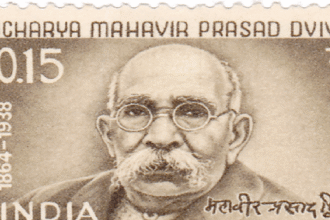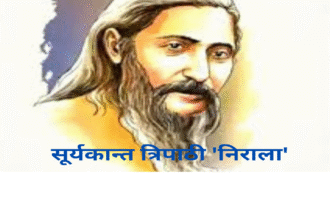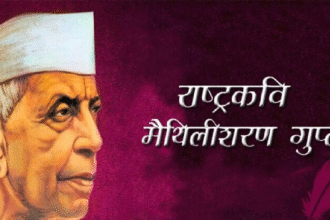संत कबीर दास भारत के सबसे महान रहस्यवादी कवि, संत और समाज सुधारक माने जाते हैं। वे अपने गहरे आध्यात्मिक ज्ञान, निडर सामाजिक आलोचना और सार्वभौमिक भाईचारे के संदेश के लिए हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी के बीच समान रूप से पूजे जाते हैं। कबीर का जीवन न केवल उनकी कविताओं और दर्शन के लिए बल्कि सामाजिक और धार्मिक कट्टरता को चुनौती देने के लिए भी अद्भुत था। उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बना हुआ है।
जन्म और प्रारंभिक जीवन
कबीर के जन्म की तिथि निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, हालांकि विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म 1398–1448 ईस्वी के बीच वाराणसी (काशी) में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उनके माता-पिता मुस्लिम जुलाहा (बुनकर) जाति से थे। उनके जन्म को लेकर कई किंवदंतियाँ हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार वे एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे जिन्होंने उन्हें त्याग दिया था और उन्हें एक गरीब मुस्लिम दंपत्ति नीरू और नीमा ने पाल-पोसकर बड़ा किया। कुछ परंपराओं में कहा जाता है कि वे दिव्य रूप से प्रकट हुए और उनके कोई जैविक माता-पिता नहीं थे।
कबीर ने बचपन से ही आध्यात्मिक झुकाव और जिज्ञासु स्वभाव दिखाया। वे बुनकर परिवार में पले और जीवन भर बुनाई का कार्य करते रहे। औपचारिक शिक्षा प्राप्त न होने के बावजूद वे असाधारण गहराई के कवि और महान विचारक बने।
आध्यात्मिक खोज और गुरु रामानंद
कबीर ईश्वर को पाने की लालसा रखते थे और एक गुरु की तलाश में थे। कथा के अनुसार उन्होंने प्रसिद्ध भक्ति संत स्वामी रामानंद के शिष्य बनना चाहा। कहा जाता है कि वे वाराणसी के पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए और जब रामानंद जी प्रातःकाल स्नान के लिए आए तो उनका पैर कबीर पर पड़ गया। रामानंद जी चौंककर बोले — “राम! राम!”। कबीर ने इसी शब्द को अपना दीक्षा मंत्र मान लिया।
यह अनूठी दीक्षा कबीर के समावेशी दर्शन को दर्शाती है। एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बाद उन्होंने एक हिंदू गुरु को स्वीकार किया लेकिन किसी भी धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर सत्य को पाया। यही उनकी शिक्षाओं का मूल आधार बना।
दर्शन और शिक्षाएँ
कबीर की शिक्षाएँ दोहों, पदों और सरल गीतों में दर्ज हैं। वे हिंदू-मुस्लिम दोनों के आडंबर और पाखंड के कटु आलोचक थे। वे लोगों से बाहर के कर्मकांडों के बजाय अपने भीतर ईश्वर को खोजने का आग्रह करते थे।
उनके दर्शन के मुख्य पहलू इस प्रकार हैं:
- एकेश्वरवाद: कबीर एक निराकार, सर्वव्यापक ईश्वर में विश्वास करते थे। वे उसे राम, अल्लाह, हरि, गोविंद जैसे अनेक नामों से पुकारते थे।
- अंतर्मुखी साधना: उन्होंने सिखाया कि सच्ची पूजा प्रेम और भक्ति से होती है, तीर्थ यात्रा, उपवास और बाहरी दिखावे से नहीं।
- जाति और भेदभाव का विरोध: उन्होंने जातिवाद और छुआछूत का कड़ा विरोध किया। उनके अनुसार सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान हैं।
- कर्मकांड की आलोचना: उन्होंने मूर्ति पूजा, ढोंग और मौलवियों व पंडितों के पाखंड का विरोध किया।
- प्रेम और करुणा: उनकी कविताएँ प्रेम, करुणा, विनम्रता और क्षमा का संदेश देती हैं।
उनका प्रसिद्ध दोहा है:
“कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माहि।
ऐसे घट-घट राम है, दुनिया देखे नाहि।”
(कस्तूरी हिरण के भीतर होती है लेकिन वह जंगल में उसे खोजता है। उसी तरह ईश्वर हर हृदय में है लेकिन लोग बाहर ढूंढते हैं।)
संत कबीर दास की रचनाएँ
संत कबीर दास ने अपनी शिक्षाओं को किसी पुस्तक में स्वयं नहीं लिखा। उन्होंने अपने विचारों को पद, दोहे और साखी के रूप में बोला, जिन्हें उनके शिष्यों ने संकलित किया। उनकी रचनाओं की भाषा साधारण थी, जिसमें अवधी, ब्रज, हिंदी और फारसी शब्दों का मिश्रण था।
सबसे प्रसिद्ध हैं उनके दोहे, जो दो पंक्तियों में गहरे जीवन और आध्यात्मिक सत्य को सरल ढंग से व्यक्त करते हैं। जैसे –
“बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय।
जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय।”
कबीर के पद भक्ति और ईश्वर से प्रेम से भरे गीत हैं, जिन्हें आज भी भजनों और कीर्तन में गाया जाता है।
उनकी शिक्षाएँ साखी और शलोक के रूप में भी मिलती हैं। उनकी रचनाओं का सबसे बड़ा संकलन बीजक कहलाता है, जो कबीर पंथियों का मुख्य ग्रंथ है। इसमें तीन भाग हैं – रामैनी, सबद (पद) और साखी। कबीर के कई पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं।
उनकी रचनाओं में जातिवाद, पाखंड और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ आवाज और निराकार ईश्वर की भक्ति का संदेश प्रमुख है। उनकी वाणी आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है।
सामाजिक सुधारक
कबीर केवल आध्यात्मिक शिक्षक नहीं बल्कि निडर समाज सुधारक भी थे। उन्होंने पाखंडी धार्मिक नेताओं और जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई। अपने बुनकर जीवन से उन्होंने श्रम की महत्ता को दर्शाया। वे उस समय में जीते थे जब समाज धार्मिक और जातीय विभाजनों से ग्रस्त था। उनके साहसी शब्द क्रांतिकारी थे। कबीर के विचारों और निडरता से उन्हें कई दुश्मन भी बने। हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के कट्टरपंथी उनसे नाराज रहते थे। शासक वर्ग ने भी उन्हें कई बार बुलवाया लेकिन वे अपने मार्ग से नहीं डिगे। कबीर के अनुयायी सभी जातियों और धर्मों के लोग बने। उनके अनुयायियों ने कबीर पंथ की स्थापना की, जो आज भी देश-विदेश में फैला हुआ है।
मृत्यु और विरासत
कबीर का निधन 1518 ईस्वी में मगहर (गोरखपुर के पास) में हुआ। एक कथा के अनुसार, उनके निधन के बाद हिंदू और मुस्लिम उनके अंतिम संस्कार के तरीके पर विवाद करने लगे। जब उनके शरीर से चादर हटाई गई तो वहां केवल फूल मिले। फूलों को दोनों ने बांट लिया, जो उनके एकता के संदेश का प्रतीक है।
भारतीय साहित्य और संस्कृति पर प्रभाव
कबीर का जीवन भारतीय साहित्य, भक्ति और सूफी परंपराओं पर अमिट छाप छोड़ गया। उनके दोहे आज भी स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं और उनकी शिक्षाएँ आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। गांधी जी, टैगोर और विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने कबीर के विचारों से प्रेरणा ली। भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किए हैं। उनकी जयंती (कबीर जयंती) हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाई जाती है। वाराणसी का कबीर चौरा मठ और मगहर का कबीरधाम उनके प्रमुख स्मारक स्थल हैं।
संत कबीर दास केवल कवि या संत नहीं बल्कि एक युगद्रष्टा थे। उन्होंने पाखंड, जातिवाद और धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। उनका जीवन सरलता, सच्चाई, प्रेम और समानता का प्रतीक है। उनके दोहे और शिक्षाएँ आज भी हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्चा धर्म दूसरों से प्रेम करना और स्वयं को जानना है। आज के समय में जब समाज में विभाजन और असहिष्णुता बढ़ रही है, कबीर का यह संदेश — “सबमें राम, सबमें रहीम” — और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। संत कबीर आज भी प्रेम, समानता और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए अनगिनत लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। वे भारतीय संस्कृति के इतिहास में हमेशा एक प्रकाशस्तंभ बने रहेंगे।