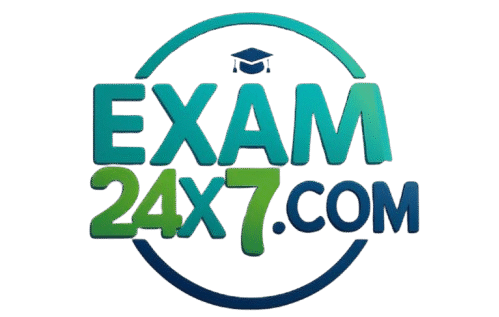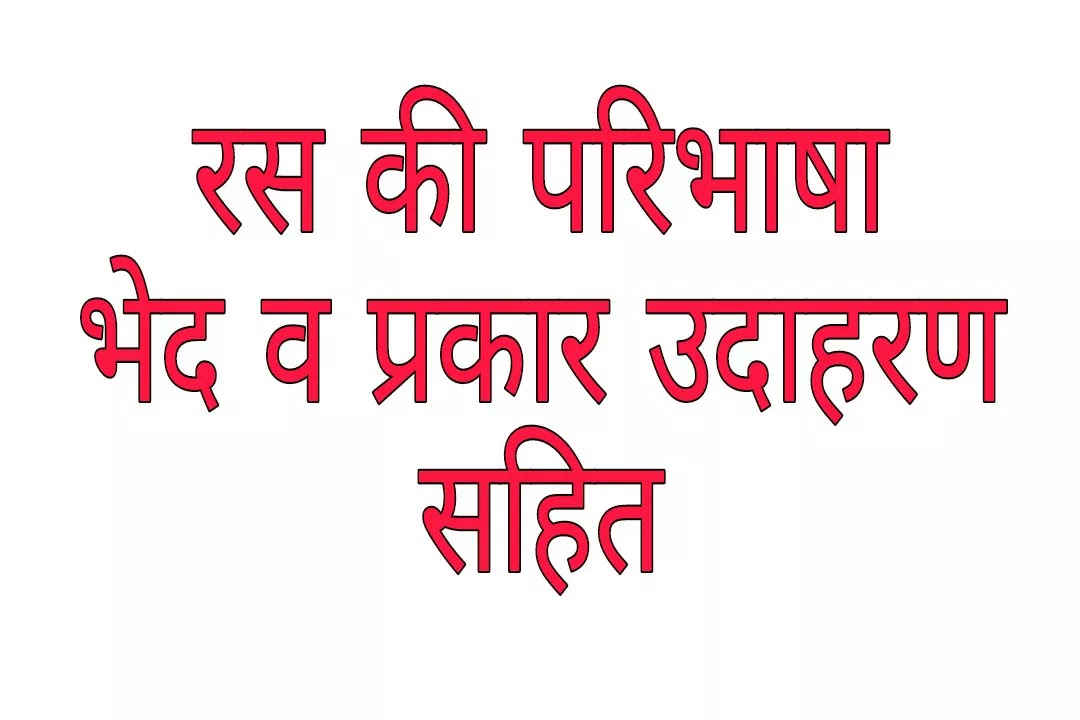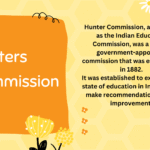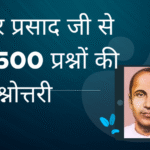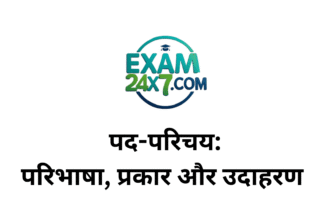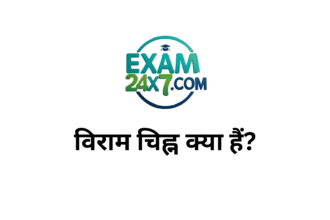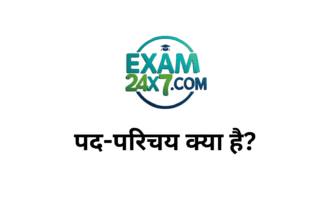हिंदी साहित्य में रस (Ras in Hindi Literature) का अर्थ है – भाव, भावना, आनंद या उत्कटता, जो किसी साहित्यिक रचना को पढ़ते, सुनते या देखते समय हृदय में उत्पन्न होती है। Ras kya hai Hindi mein – यह एक शास्त्रीय साहित्यिक तत्व है, जिसका प्रयोग कविता, नाटक, गीत और अन्य रचनाओं में भावनाओं को अभिव्यक्त करने हेतु किया जाता है। रस का उद्देश्य है रसिकों को सुंदरता, आनंद और संतोष का अनुभव कराना। Types of Ras in Hindi में प्रमुख हैं – शृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, वीभत्स रस और अद्भुत रस।
हिंदी साहित्य में रस क्या है? (Ras kya hai Hindi mein)
हिंदी साहित्य में रस (Ras in Hindi Literature) एक महत्वपूर्ण काव्य तत्व है, जो पाठक या श्रोता के मन में भावनात्मक अनुभव (Emotional Experience) उत्पन्न करता है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव (Sthayi Bhav) होता है, जो उस रस की मुख्य भावना (Primary Emotion) को दर्शाता है। उदाहरणस्वरूप, शृंगार रस का स्थायी भाव ‘रति’ (प्रेम) है, जबकि वीर रस में ‘उत्साह’ प्रमुख होता है। इस तालिका में 11 प्रमुख रसों और उनके स्थायी भावों को दर्शाया गया है, जो विद्यार्थियों और परीक्षार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह ज्ञान प्रतियोगी परीक्षाओं एवं साहित्य अध्ययन में सहायक सिद्ध होता है। रस का मुख्य उद्देश्य होता है रसिकों को सुंदरता, आनंद और संतोष का अनुभव कराना। हिंदी साहित्य में रस के मुख्य प्रकार (Types of Ras in Hindi) हैं —
| क्रम | रस का नाम | स्थायी भाव (Sthayi Bhav) |
| 1. | शृंगार रस | रति (प्रेम) |
| 2. | हास्य रस | हास (हास्य) |
| 3. | करुण रस | शोक (दुःख) |
| 4. | रौद्र रस | क्रोध |
| 5. | वीर रस | उत्साह |
| 6. | भयानक रस | भय |
| 7. | वीभत्स रस | जुगुप्सा (घृणा) |
| 8. | अद्भुत रस | विस्मय (आश्चर्य) |
| 9. | शांत रस | निर्वेद (वैराग्य) |
| 10. | वात्सल्य रस | वात्सल्य (ममता/स्नेह) |
| 11. | भक्ति रस | श्रद्धा (भक्ति, समर्पण भाव) |
1- शृंगार रस की परिभाषा (Shringar Ras in Hindi Literature)
शृंगार रस (Shringar Ras in Hindi Literature) को रसों का राजा कहा जाता है। Shringar Ras kya hai – यह रस प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण की भावनाओं को व्यक्त करता है। इसमें प्रेम (Love), माधुर्य (Sweetness), सौंदर्य (Beauty) और आकर्षण (Attraction) की अनुभूति प्रमुख होती है। शृंगार रस के दो रूप होते हैं – संयोग शृंगार (Union) और वियोग शृंगार (Separation)। इसका उद्देश्य है पाठक या दर्शक के हृदय में कोमल, मधुर और रोमांचक भाव उत्पन्न करना। Shringar Ras in Hindi Literature का प्रयोग खासकर कविता, नाटक और गीतों में अधिक होता है।
शृंगार रस के प्रसिद्ध उदाहरण (Famous Examples of Shringar Ras)
यहाँ शृंगार रस के 4 उदाहरण पूरे दोहे / पदों के साथ दिए जा रहे हैं, जिनमें प्रेम, माधुर्य और सौंदर्य का भाव स्पष्ट है —
1. राधा-कृष्ण का रास लीला
“मोर मुकुट सिर, कानन कुंडल, बनमाल बिचि देह सुहाई।
सुरतरु अंजन, मृदु मुरली धुनि, राधा संग रास रचाई।”
भाव – यहाँ कृष्ण के सौंदर्य और राधा के साथ रास का वर्णन है, जो संयोग शृंगार का उत्कृष्ट उदाहरण है।
2. सीता-राम का मिलन
“सीय राममय सब जग जानी, करहुँ प्रनाम जोरि जुग पानी।
सकल सुमंगल दायक राजा, रघुकुल तिलक राम सुख साजा।” (गोस्वामी तुलसीदास)
भाव – अयोध्या में राम और सीता के मिलन के समय की पावन एवं मधुर भावना।
3. मीरा का कृष्ण के प्रति प्रेम
“मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई।
जा के सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई।”
भाव – मीरा का एकनिष्ठ और माधुर्यपूर्ण प्रेम कृष्ण के प्रति, जो भक्ति शृंगार का अद्वितीय उदाहरण है।
4. जयदेव की ‘गीत गोविंद’
“स्मरामि माधवम्, राधिका-रमणम्, जयदेवकृतम्।
कुसुमित वनराजि-मनोहरम्, मृगमद-गन्ध-लसत्-तनुम्।”
भाव – वसंत ऋतु में राधा-कृष्ण के मनोहर मिलन का चित्रण, जिसमें सौंदर्य और प्रेम का उत्कर्ष है।
2- वीर रस की परिभाषा (Veer Ras in Hindi Literature)
वीर रस (Veer Ras in Hindi Literature) हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण रस है, जो साहस, पराक्रम और वीरता की भावना को प्रकट करता है। Veer Ras में नायक या पात्र कठिन परिस्थितियों में भी निर्भीक, दृढ़ और न्याय के प्रति समर्पित दिखाई देता है। यह रस पाठक या श्रोता के मन में उत्साह, जोश और गौरव की अनुभूति कराता है। Ras in Hindi की यह श्रेणी विशेष रूप से महाकाव्यों, युद्ध वर्णनों और ऐतिहासिक कविताओं में पाई जाती है। Veer Ras ke prakar में मुख्यतः दानवीर, दयावीरा, युद्धवीरा और धर्मवीरा आते हैं, जो अपने आदर्शों और साहस से प्रेरणा देते हैं।
वीर रस के प्रसिद्ध उदाहरण (Famous Examples of Veer Ras)
1. आल्हा-ऊदल (आल्हा खंड से)
“सिर कटि जाय पर भगि न जावैं, रण छूटि न जावैं वीर।
धरा रहै धरा की धाक, गगन रहै गगन की नीर॥”
भाव – सच्चा वीर प्राण भले ही दे दे, पर रणभूमि से पीठ नहीं दिखाता।
2. छत्रपति शिवाजी पर (भूषण कवि)
“सिंहासन हिल उठे, गूँज उठे रण के नारे।
भीषण होकर गिरे, भूषण के शेर हमारे॥”
भाव – रणभूमि में वीरों का आगमन शत्रु के दिल में भय पैदा करता है।
3. महाराणा प्रताप पर
“चलत गज पंक्ति जैसे वन में गर्जै महा सिंह।
महाराणा प्रताप के सम नहिं रण में कोई अन्य॥”
भाव – महाराणा प्रताप का शौर्य और उनके युद्ध कौशल का बखान।
4. गुरु गोविंद सिंह (स्वयं की वाणी)
“सवा लाख से एक लड़ाऊँ,
चिद्द करूँ रण में।
निश्चय कर अपनी जीत करूँ,
सिक्खों की शान बढ़ाऊँ॥”
भाव – अपार साहस, अल्प सेना से भी शत्रु को परास्त करने का संकल्प।
3- करुण रस की परिभाषा (Karuna Ras in Hindi Literature)
करुण रस (Karuna Ras) हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण रस (Rasa) है, जो दुःख (Sorrow), वियोग (Separation), विपत्ति (Misfortune) और संवेदना (Sensitivity) की भावनाओं को व्यक्त करता है। यह रस पाठक या श्रोता के मन में दया (Compassion), शोक (Grief) और सहानुभूति (Sympathy) उत्पन्न करता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक (Shoka) होता है। कवि करुण रस का प्रयोग युद्ध, प्रेम-वियोग, मृत्यु, या विपत्ति की घटनाओं को चित्रित करने में करता है, ताकि पाठक के मन में कोमल भावनाएँ जाग्रत हों। हिंदी साहित्य में तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि कवियों ने करुण रस की मार्मिक रचनाएँ प्रस्तुत की हैं।
करुण रस के प्रसिद्ध उदाहरण (Famous Examples of Karun Ras)
1. तुलसीदास – रामचरितमानस
भरत मिलाप प्रसंग
बंधु बियोग सुनि अति दुःखी, भरत गए बन आइ।
बिनु राम तनु प्रान सम, जनु जल बिनु मीनाई॥
भावार्थ: भरत अपने भाई राम के वियोग में अत्यंत दुःखी होकर वन में पहुँचते हैं। राम के बिना वे स्वयं को ऐसे महसूस करते हैं जैसे जल के बिना मछली।
2. सूरदास – श्रीकृष्ण लीलाएं
मां यशोदा का शोक
मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो।
मछली खायन बोल्यो, कहि ग्वालिन सब को बतायो॥
भावार्थ: बाल कृष्ण की शिकायत लेकर दाऊ (बलराम) यशोदा के पास आते हैं, और यह सुनकर यशोदा के मन में पीड़ा और चिंता जागती है।
3. मीराबाई – भक्ति पद
श्रीकृष्ण विरह
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, किरपा कर अपनायो॥
भावार्थ: मीरा अपने आराध्य श्रीकृष्ण के वियोग में उनके नाम को ही सबसे बड़ा धन मानती हैं, विरह की पीड़ा उनके भावों में झलकती है।
4. कबीरदास – विरह पीड़ा
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय।
जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय॥
भावार्थ: कबीर बताते हैं कि लोग दुख में ही भगवान को याद करते हैं, जबकि सुख में कोई याद नहीं करता। यह मानव स्वभाव की करुण स्थिति को व्यक्त करता है।
4- हास्य रस की परिभाषा (Hasya Ras in Hindi Literature)
हास्य रस (Hasya Ras) साहित्य और कविता में आनंद (Joy) तथा मनोरंजन (Entertainment) उत्पन्न करने वाला प्रमुख रस है। इसका उद्देश्य हँसी (Laughter) और प्रसन्नता (Happiness) की अनुभूति कराना होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास (Has) है, जिसमें पात्रों की विनोदी (Humorous), व्यंग्यात्मक (Satirical) या मजाकिया (Comical) गतिविधियाँ पाठक या श्रोता को आनंदित करती हैं। यह रस अक्सर संवाद (Dialogue), अतिशयोक्ति (Exaggeration), त्रुटि (Mistake) या विनोदपूर्ण स्थितियों (Funny Situations) से उत्पन्न होता है। हास्य रस का प्रयोग न केवल मनोरंजन के लिए, बल्कि सामाजिक संदेश (Social Message) देने हेतु भी किया जाता है, जिससे यह शिक्षाप्रद और रोचक दोनों बनता है।
हास्य रस के प्रसिद्ध उदाहरण (Famous Examples of Hasya Ras)
इन हास्य रस के दोहों के रचयिता काका हाथरसी हैं। काका हाथरसी (1906–1995) हास्य-व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध कवि थे, जिनकी रचनाओं में समाज के विभिन्न पहलुओं पर हल्के-फुल्के अंदाज़ में कटाक्ष मिलता है।
दोहा 1
लाला की लाली यों बोली,
सारा खाना यह चर जाएंगे।
ये जो बच्चे भूखे बैठे हैं,
क्या पंडित जी को खिलाएंगे।
भावार्थ: यह दोहा हास्य रस से भरपूर है। इसमें पंडित जी के अधिक खाने की आदत पर मज़ाक किया गया है। कवि कहता है कि पंडित जी सारा भोजन स्वयं खा जाएंगे, तो जो बच्चे भूखे बैठे हैं, उन्हें कौन खिलाएगा?
दोहा 2
हाथी जैसी देह, गैडे जैसी खाल
तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से बाल।
भावार्थ: इस दोहे में एक व्यक्ति के शरीर का हास्यपूर्ण वर्णन है। कवि ने तुलना करते हुए कहा है कि उसका शरीर हाथी जैसा बड़ा, त्वचा गैंडे जैसी मोटी, सिर तरबूजे जैसा और बाल खरबूजे जैसे हैं।
दोहा 3
सिरा पर गंगा हँसे, भुजिन में भुजंगा हँसे
हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में।
भावार्थ: इस दोहे में कवि कहता है कि नंगे व्यक्ति के विवाह में सभी हँसी-मज़ाक कर रहे हैं। यहाँ तक कि सिर पर गंगा (बाल) और भुजाओं में भुजंग (साँप जैसी नसें) भी हँस रही हैं। दृश्य इतना अजीब है कि पूरा माहौल हँसी में बदल गया है।
दोहा 4
जौई जहाँ देखे सो हँसे है, ताई राह में!
मगन भए इस हँसे, नंगन महेश ठाकुर।
और हँसे एक हँसी हँसी के उमाह में!
भावार्थ: इसमें हास्य रस की चरम सीमा दिखाई देती है। महेश ठाकुर नामक व्यक्ति अपनी हरकतों से सभी को हँसा रहा है। जो भी उसे देखता है, हँसी रोक नहीं पाता और हँसी का माहौल पूरे रास्ते फैल जाता है।
5- रौद्र रस (Raudra Ras) – परिभाषा (Definition of Raudra Ras)
रौद्र रस (Raudra Ras) संस्कृत साहित्य और हिंदी काव्य में क्रोध (Anger) एवं प्रतिशोध (Revenge) की तीव्र भावना को व्यक्त करने वाला रस है। यह रस तब उत्पन्न होता है जब नायक या पात्र को अन्याय (Injustice), अपमान (Insult) या अत्याचार (Oppression) का अनुभव होता है। इसमें वीरता (Bravery) और आक्रोश (Wrath) का संगम दिखाई देता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, जो शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों में प्रकट होता है। कवि रौद्र रस के माध्यम से अन्याय के विरुद्ध संघर्ष (Struggle) और शत्रु पर विजय (Victory over Enemy) की तीव्र इच्छा को व्यक्त करते हैं, जिससे पाठक में उत्तेजना और जोश जागृत होता है।
रौद्र रस के प्रसिद्ध उदाहरण (Famous Examples of Raudra Ras)
लेखक: रामधारी सिंह ‘दिनकर’
दोहा:
उस काल मरे क्रोध के तन काँपने उसका लगा।
मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा।।
भाव: यहाँ कवि ने क्रोध की तीव्रता का वर्णन किया है, जो शरीर में कंपन पैदा कर देता है और सोए हुए समुद्र की तरह प्रचंड हो उठता है।
2. लेखक: अशोक चक्रधर
दोहा:
भारत का भूगोल तड़पता, तड़प रहा इतिहास है।
तिनका–तिनका तड़प रहा है, तड़प रही हर सांस है।
सिसक रही है सरहद सारी, मां के छाले कहते हैं।
ढूंढ रहा हूं किन गलियों में, अर्जुन के सूत रहते हैं।।
भाव: यह पंक्तियाँ देश की वर्तमान पीड़ा और वीरों की कमी को दर्शाती हैं, जहाँ हर कोना संघर्ष और आंसुओं से भरा है।
3. लेखक: अज्ञात (लोककाव्य शैली)
दोहा:
उबल उठा शोणित अंगो का, पुतली में उत्तरी लाली।
काली बनी स्वयं वह बाला, अलक-अलक विषधर काली।।
भाव: यहाँ क्रोध से भरी एक बाला का चित्रण है, जिसकी आंखों में लालिमा और बालों में नागिन जैसी तीक्ष्णता है।
6- भयानक रस की परिभाषा (Bhayanak Ras in Hindi Literature)
भयानक रस (Bhayanak Ras) साहित्य और नाट्यकला का वह स्थायी भाव है जिसमें भय (Fear) और आतंक (Terror) की अनुभूति कराई जाती है। इसका स्थायी भाव भय है, जो विभत्स या भयानक घटनाओं के चित्रण से उत्पन्न होता है। जब पाठक या दर्शक किसी हिंसक दृश्य (Violent Scene), मृत्यु (Death), अलौकिक घटना (Supernatural Event) या प्रलयकारी आपदा (Catastrophe) को देखकर डर और घबराहट महसूस करता है, तब भयानक रस उत्पन्न होता है। इस रस में करुण (Compassion) और विभत्स (Disgust) का मिश्रण भी पाया जा सकता है। इसे प्रायः युद्ध, दैत्य-वध, राक्षस, भूत-प्रेत और आपदा-प्रसंगों में प्रयोग किया जाता है।
भयानक रस के प्रसिद्ध उदाहरण (Famous Examples of Bhayanak Ras)
(1) लेखक: सुमित्रानंदन पंत
दोहा: अखिल यौवन के रंग उमर, हड्डियों के हिलाते कंकाल।
कचो के चिकने काले, व्याल, केंचुली, कौंस, सिवार।।
भाव: यह पंक्तियाँ मृत्यु की भयानकता और जीवन के अंत का सजीव चित्रण करती हैं, जिसमें यौवन का सौंदर्य कंकाल और भयावह दृश्यों में बदल जाता है।
(2) लेखक: सुमित्रानंदन पंत
दोहा: उधर गरजति सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालौं सी।
चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाये व्यालौं सी।।
भाव: समुद्र की गर्जना और उसकी लहरों की भयावहता को फन फैलाए सर्प के रूप में दर्शाया गया है, जो विनाश का संकेत देती हैं।
(3) लेखक: सूरदास
दोहा: सुभिन साजि पड़ाव है निज फौज लखे मरहधुन केरी।
औंरंग आपुनि दुग्ग जमाति बिलोकत तेरी फौज डेरी।।
भाव: यहाँ युद्ध की तैयारी और शत्रु की विशाल सेना का वर्णन है, जिसमें रणभूमि की गंभीरता और चुनौती की अनुभूति होती है।
(4) लेखक: हरिवंश राय बच्चन
दोहा: आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात!
चार दिन सुखद चाँदनी रात और फिर अन्धकार, अज़ालात!
भाव: जीवन के छोटे और सुखद क्षणों के बाद आने वाले बुढ़ापे और अंत का मार्मिक चित्रण है।
(5) लेखक: मैथिलीशरण गुप्त
दोहा: पुनि किलकिल समुद्र महं आए, गा धीरज देखत डर खाए।
या किलकिल अरु या उठे हिलोरे, संग अकस टूटे अंधारे।।
भाव: समुद्र के उफान और उसमें उठती लहरों का वर्णन है, जिसमें डर, रोमांच और प्रकृति की प्रचंड शक्ति का एहसास होता है।
7- वीभत्स रस (Vibhats Ras) – परिभाषा
वीभत्स रस (Vibhats Ras) संस्कृत काव्यशास्त्र का एक प्रमुख भावात्मक रस (Emotional Rasa) है, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा (Disgust) होता है। जब किसी वस्तु, दृश्य, घटना या आचरण को देखकर मन में घृणा (Hatred), वितृष्णा (Repulsion) या अरुचि (Aversion) उत्पन्न होती है, तब वीभत्स रस की अनुभूति होती है। इसका आलंबन (Alamban) घृणित वस्तु या परिस्थिति, उद्दीपन (Uddipan) उसका वातावरण, और अनुभाव (Anubhav) मुँह फेरना, नाक सिकोड़ना, वमन की भावना आदि होते हैं। साहित्य में वीभत्स रस का प्रयोग प्रायः युद्ध, मृत्यु, रोग, हिंसा, अपवित्रता और कुरूपता (Ugliness) के चित्रण में किया जाता है, जिससे पाठक के मन में घृणा उत्पन्न हो।
वीभत्स रस के प्रसिद्ध उदाहरण (Famous Examples of Vibhats Ras)
दोहा:
आँखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ कर आ जाते
शव जीभ खींचकर कौवे, चुपला-चपला कर खाते
भाव: यह दृश्य शवभक्षण करते पक्षियों का वीभत्स चित्रण है, जिससे घृणा और वितृष्णा उत्पन्न होती है।
दोहा:
सिर पर बैठी काग, आँखि दौड़ खाट निकालत
गिद्ध जाँघ कह खोद-खोद के मांस उचारत
भाव: यहाँ मृत शरीर को नोचते गिद्ध और कौओं का वर्णन है, जो वीभत्स रस को तीव्रता से प्रकट करता है।
दोहा:
बहु चील्त नौंचि ले जात तुझ, मूर्द मच्यो सबको हियो
जणु ब्रह भोज जिजमान को, आज भिखारिन कहूँ दियो
भाव: यह दृश्य शव को नोचते पक्षियों और पशुओं का वर्णन करता है, जिससे गहरी घृणा का अनुभव होता है।
8- अद्भुत रस की परिभाषा (Adbhut Ras in Hindi)
अद्भुत रस (Adbhut Ras) संस्कृत काव्यशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भावात्मक रस (Emotional Rasa) है, जिसका स्थायी भाव आश्चर्य (Wonder/Amazement) होता है। जब किसी असामान्य, विलक्षण, अद्वितीय या अद्भुत घटना, दृश्य, वस्तु या कार्य को देखकर मन में चमत्कार (Marvel), विस्मय (Astonishment) या कौतूहल (Curiosity) उत्पन्न होता है, तब अद्भुत रस की अनुभूति होती है। इसका आलंबन (Alamban) आश्चर्यजनक वस्तु या घटना, उद्दीपन (Uddipan) उसका विलक्षण वातावरण, और अनुभाव (Anubhav) विस्मित नेत्र, मुख खुला रह जाना, हर्ष या कौतूहल से भर उठना आदि होते हैं। साहित्य और कला में यह रस पाठक या दर्शक के मन को आकर्षण और विस्मय से भर देता है।
अद्भुत रस के प्रसिद्ध उदाहरण (Famous Examples of Adbhut Ras)
दोहा:
चित अलि कत भरमत रहत कहाँ नहीं बासा।
विकसित कुसुमन में अहे काको सरस विकासा।।
भाव: यहाँ खिले हुए पुष्प में भंवरे की चंचलता और आकर्षण को देखकर अद्भुत रस व्यक्त हुआ है, जो सौंदर्य और विस्मय का अनुभव कराता है।
दोहा:
देख यशोदा शिशु के मुख में, सकल विश्व की माया,
क्षणभर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया।।
भाव: श्रीकृष्ण के मुख में सम्पूर्ण ब्रह्मांड का दृश्य देखकर माता यशोदा विस्मित हो जाती हैं, जो अद्भुत रस की चरम अनुभूति है।
लेखक: तुलसीदास
दोहा:
देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखण्ड,
रोम रोम प्रति लगे कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड।
भाव: भगवान राम के विराट और अद्वितीय रूप को देखकर माता कैकेयी अद्भुत विस्मय से भर जाती हैं, जो अद्भुत रस का उदाहरण है।
9- शांत रस की परिभाषा (Definition of Shant Ras in Hindi)
शांत रस (Shant Ras) हिंदी साहित्य का एक प्रमुख आध्यात्मिक रस (Spiritual Ras) है, जिसका स्थायी भाव (Sthayi Bhav) निर्वेद या वैराग्य (Detachment) होता है। जब व्यक्ति संसार की माया, दुःख और सुख से ऊपर उठकर शांति (Peace), संतोष (Contentment) और आत्मिक ज्ञान (Self-realization) की ओर अग्रसर होता है, तब शांत रस की अनुभूति होती है। यह रस विशेषतः भक्ति काव्य (Bhakti Poetry) और ज्ञानमार्गी साहित्य (Philosophical Literature) में प्रकट होता है। शांत रस का उद्देश्य पाठक या श्रोता के मन में वैराग्य, धैर्य, और आध्यात्मिक स्थिरता उत्पन्न करना है।
शांत रस के प्रसिद्ध उदाहरण (Famous Examples of Shant Ras)
1. कबीर दास
मन लागो यार फ़कीरी में, धन दौलत में मन नाहीं।
जो सुख पाओ दरवेशी में, सो राज न लख पाई।
भाव: यहाँ कबीर ने फकीरी और वैराग्य को राजसुख से श्रेष्ठ बताया है।
2. तुलसीदास
तुलसी इस संसार में, भांति-भांति के लोग।
सबसे हस मिल बोलिए, नदी नाव संजोग।।
भाव: तुलसीदास जी संसार को अस्थायी मानते हुए सबके साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार की बात करते हैं।
3. रहीम
रहिमन विपदा हू भली, जो थोरे दिन होय।
हित अनहित या जगत में, जानि परत सब कोय।।
भाव: रहीम कहते हैं कि विपत्ति में ही मनुष्य को संसार का यथार्थ ज्ञान होता है।
4. सूरदास
सूरदास यह जग बौराना, कोऊ न सकल समुझाना।
ज्यों-ज्यों दिन बीतत है, मन वैराग्य में रमाना।।
भाव: सूरदास इस दोहे में जीवन की नश्वरता और वैराग्य की ओर बढ़ने की बात करते हैं।
10- वात्सल्य रस की परिभाषा (Definition of Vatsalya Ras in Hindi)
वात्सल्य रस (Vatsalya Ras) हिंदी साहित्य का एक ममत्वपूर्ण और स्नेहपूर्ण रस है, जिसमें माता-पिता और संतान (Parent–Child) के बीच के प्रेम (Affection), स्नेह (Tenderness) और ममता (Motherly Love) को व्यक्त किया जाता है। इसका स्थायी भाव (Sthayi Bhav) वात्सल्य होता है। इस रस में नायक या पात्र को शिशु रूप में देखा जाता है और उसके प्रति पालक का स्नेह, चिंता व प्रेम उभर कर आता है। यह रस विशेष रूप से भक्ति साहित्य में प्रयुक्त होता है, जहाँ ईश्वर को बाल रूप (Child Form of God) में दर्शाकर उसके प्रति मातृत्व भाव प्रकट किया जाता है। यशोदा-कृष्ण के प्रसंग इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं।
वात्सल्य रस के प्रसिद्ध उदाहरण (Famous Examples of Vatsalya Ras)
1. सूरदास (यशोदा और कृष्ण का संवाद)
मैया मोरी मैं नहिं माखन खायो।
बल लै माता कबहुँ न डारो, मोहिं डर लागो।।
भाव: यहाँ कृष्ण बाल रूप में हैं और अपनी माँ यशोदा से बाल-भाव में माखन न खाने का नाटक कर रहे हैं। माँ की ममता और शिशु की चंचलता दोनों व्यक्त हैं।
2. तुलसीदास (राम की बाल लीलाएँ)
सुनत जशु अति पुलक सरीरा, राम लखन बैठें गोदीं लीरा।
माता कौसल्या हरषि समाना, देखि सुभग मुख बिमल विधाना।।
भाव: माता कौसल्या राम और लक्ष्मण को गोद में खेलते देख आनंद से भर जाती हैं — यह वात्सल्य रस का सुंदर चित्रण है।
3. सूरदास (कृष्ण की बाल लीलाएँ)
लली! जसोदा बउरी भई री!
कृष्ण को कछु न कहत हठी री, बाँधत नंद कंवर कटी री!
भाव: यशोदा अपने पुत्र कृष्ण की शरारतों से परेशान हो गई हैं, लेकिन उन्हें डाँटना भी नहीं चाहतीं — यही वात्सल्य है।
4. मीरा बाई (कृष्ण को पुत्र रूप में देखना)
पायो जी मैंने गोपाल लला।
सुनत धुनि बिनु बाजे, मोरे अंगना बजै मुरला।।
भाव: मीरा यहाँ भगवान कृष्ण को अपने लला (बेटे) के रूप में अनुभव कर रही हैं — यह वात्सल्य और भक्ति दोनों का मेल है।
11- भक्ति रस की परिभाषा (Definition of Bhakti Ras in Hindi)
भक्ति रस (Bhakti Ras) हिंदी साहित्य का अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक रस (Spiritual Ras) है, जिसमें भक्त और भगवान के बीच के श्रद्धा, समर्पण और प्रेम (Devotion, Faith, Love) को अभिव्यक्त किया जाता है। इसका स्थायी भाव (Sthayi Bhav) श्रद्धा (Faith) अथवा भक्ति भाव (Devotion) होता है। यह रस मुख्य रूप से भक्ति काल (Bhakti Kaal) की रचनाओं में देखने को मिलता है, जहाँ कवि स्वयं को दास और ईश्वर को स्वामी (Servant–Lord Relationship) मानते हैं। भक्ति रस के दो प्रमुख रूप होते हैं – सगुण भक्ति (God with form) और निर्गुण भक्ति (God without form)। तुलसीदास, सूरदास, मीरा और कबीर इसके प्रमुख कवि हैं।
1. सूरदास – श्रीकृष्ण भक्ति
मैं तो दीन दयाल को, और न कोऊ नाम।
जो सांचे मन लायिहै, ताको लेहिं थाम।।
भाव: सूरदास कहते हैं कि वह केवल श्रीकृष्ण को पुकारते हैं और ईश्वर सच्चे भक्त को कभी नहीं छोड़ते।
2. मीरा बाई – आत्मसमर्पण भाव
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो।।
भाव: मीरा अपने आराध्य को अमूल्य रत्न मानती हैं और उन्हें पाकर स्वयं को धन्य समझती हैं।
3. कबीरदास – निर्गुण भक्ति
मन ना रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा।
आसन मारि मंदिर में बैठा, नाम जपै मुँह बाड़ा।।
भाव: कबीर बाहरी आडंबर को नकारते हुए कहते हैं कि सच्ची भक्ति मन से होती है, कपड़ों और रीति से नहीं।
रस (Ras) हिंदी साहित्य का एक मूल आधार है, जिसमें शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयांक, वीभत्स, अद्भुत आदि सभी रसों का अध्ययन Competitive Exams के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है। UPSC, SSC, IBPS, SBI PO, SBI Clerk, RRB, CTET, UPTET, KVS, NVS, DSSSB, UP Police, MP Police, REET, HPTET और अन्य Government Exams में हिंदी साहित्य से जुड़े प्रश्न नियमित रूप से पूछे जाते हैं। Exam24x7.com आपको सभी रसों की परिभाषा, उदाहरण, व्याख्या, MCQs, Previous Year Papers और Mock Tests हिंदी व English दोनों में प्रदान करता है, जिससे आपकी तैयारी (Exam Preparation) मजबूत, सटीक और परीक्षा-उन्मुख बनती है।
हिंदी साहित्य में रस: FAQs
- प्रश्न: रस क्या है हिंदी साहित्य में?
उत्तर: रस वह भाव है जो साहित्य पढ़ते या सुनते समय पाठक के हृदय में उत्पन्न होता है। - प्रश्न: रस के कितने प्रकार होते हैं?
उत्तर: हिंदी साहित्य में रस के मुख्यतः 8 प्रकार होते हैं — शृंगार, वीर, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक, वीभत्स और अद्भुत। - प्रश्न: रसों का स्थायी भाव क्या होता है?
उत्तर: प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, जैसे वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। - प्रश्न: शृंगार रस क्या दर्शाता है?
उत्तर: शृंगार रस प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण की भावना को व्यक्त करता है। - प्रश्न: करुण रस कब उत्पन्न होता है?
उत्तर: करुण रस दुःख, वियोग या शोकपूर्ण घटनाओं से उत्पन्न होता है। - प्रश्न: हास्य रस किस भाव से जुड़ा है?
उत्तर: हास्य रस आनंद और हँसी की अनुभूति कराता है, इसका स्थायी भाव “हास” है। - प्रश्न: रौद्र रस का उपयोग किसमें होता है?
उत्तर: रौद्र रस क्रोध, प्रतिशोध और अन्याय के विरोध को दर्शाने के लिए होता है। - प्रश्न: अद्भुत रस किस पर आधारित है?
उत्तर: अद्भुत रस आश्चर्य और चमत्कार से उत्पन्न होता है। - प्रश्न: वीभत्स रस का क्या प्रभाव होता है?
उत्तर: वीभत्स रस घृणा, वितृष्णा और अरुचि की भावना जगाता है।
प्रश्न: रस का महत्व क्या है साहित्य में?
उत्तर: रस साहित्य में भावों की गहराई लाकर पाठक को मानसिक आनंद और जुड़ाव प्रदान करता है।